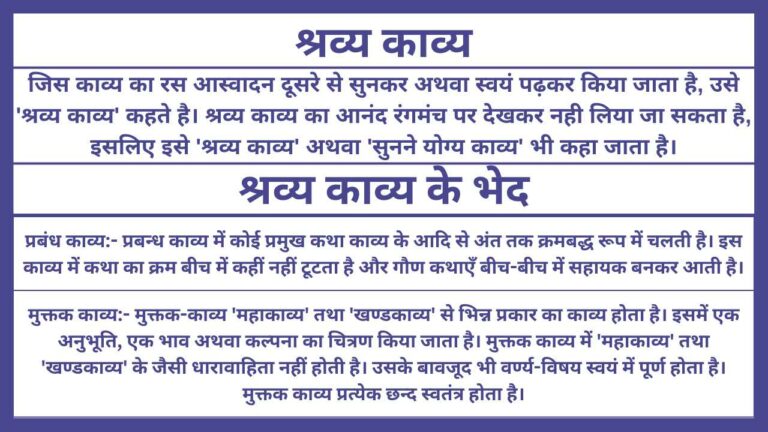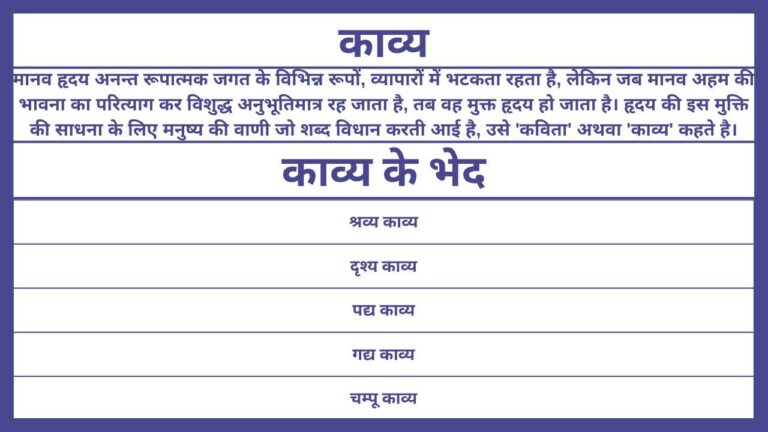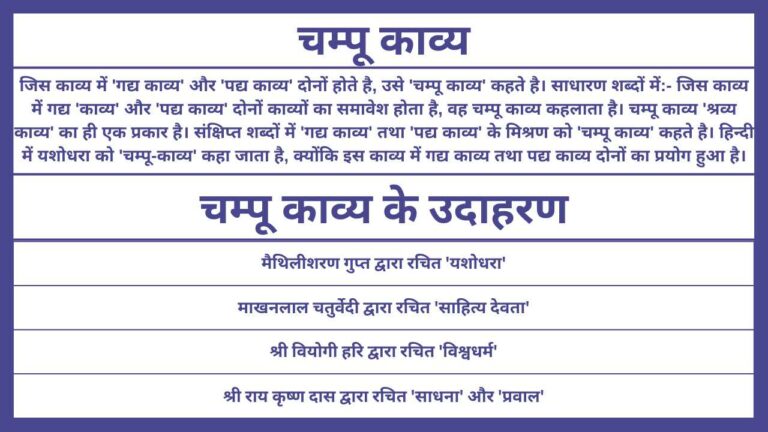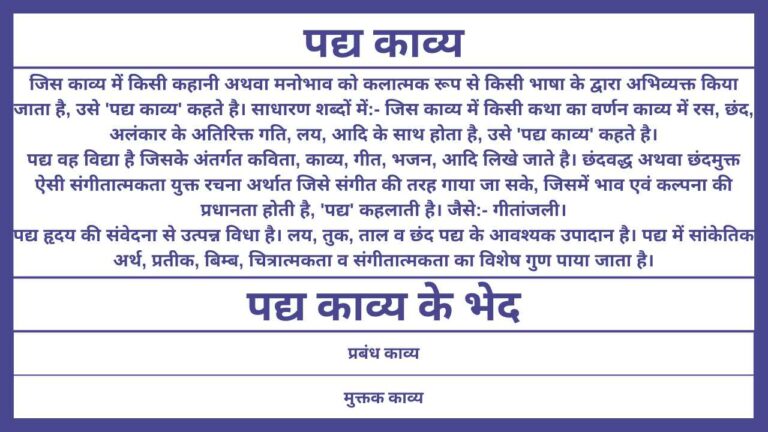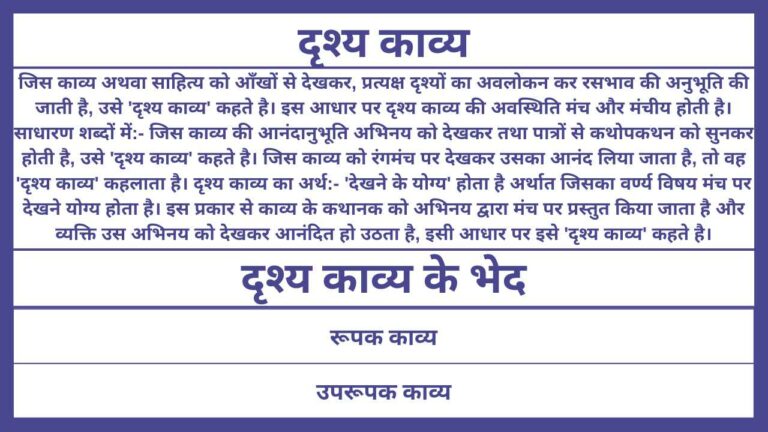गद्य काव्य की परिभाषा, भेद और उदाहरण
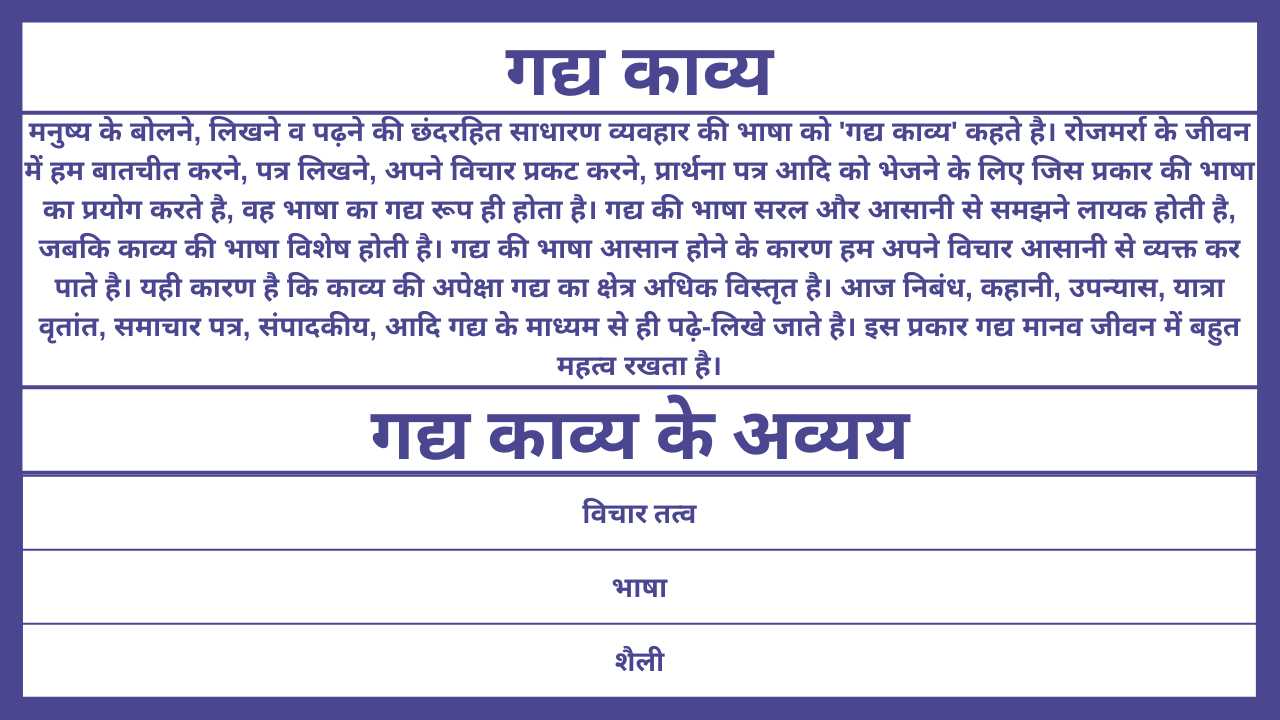
गद्य काव्य की परिभाषा : Gadya Kavya in Hindi:- आज के इस लेख में हमनें ‘गद्य काव्य की परिभाषा’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है। यदि आप गद्य काव्य से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-
गद्य काव्य की परिभाषा : Gadya Kavya in Hindi
मनुष्य के बोलने, लिखने व पढ़ने की छंदरहित साधारण व्यवहार की भाषा को ‘गद्य काव्य’ कहते है। रोजमर्रा के जीवन में हम बातचीत करने, पत्र लिखने, अपने विचार प्रकट करने, प्रार्थना पत्र आदि को भेजने के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते है, वह भाषा का गद्य रूप ही होता है।
गद्य की भाषा सरल और आसानी से समझने लायक होती है, जबकि काव्य की भाषा विशेष होती है। गद्य की भाषा आसान होने के कारण हम अपने विचार आसानी से व्यक्त कर पाते है।
यही कारण है कि काव्य की अपेक्षा गद्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। आज निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, समाचार पत्र, संपादकीय, आदि गद्य के माध्यम से ही पढ़े-लिखे जाते है। इस प्रकार गद्य मानव जीवन में बहुत महत्व रखता है।
गद्य काव्य के उदाहरण
गद्य काव्य के उदाहरण निम्नलिखित है:-
| गद्य काव्य के उदाहरण |
|---|
| जयशंकर की ‘कमायनी’ |
हिंदी गद्य का विकास
सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम हिंदी गद्य के विकास तथा प्रयोग का प्रयास ‘फोर्ट विलियम कॉलेज’ की स्थापना के बाद अंग्रेज शासकों द्वारा किया गया था।
हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 50 वर्षों में हिंदी गद्य को आगे बढ़ने में पत्र-पत्रिकाओं ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोलकाता से ‘उदंत मार्तंड’ नामक पत्र निकालना प्रारंभ हुआ।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण प्रेम धन, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल राम गहमरी, अंबिकादत्त व्यास, देवकीनंदन खत्री, आदि ने नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, आदि गद्य साहित्य की रचना की।
गद्य के अवयव
गद्य के कुल 3 अव्यय होते है, जो कि निम्नलिखित है:-
| गद्य के अव्यय |
|---|
| विचार तत्व |
| भाषा |
| शैली |
1. विचार तत्व
किसी भी गद्य रचना में विचार तत्व मुख्य होता है, चाहे वह निबंध तथा कहानी हो या उपन्यास हो। इस विचार तत्व का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि रचना के रचनाकार के बारे में पहले जानकारी प्राप्त की जाए कि वह किस काल के रचनाकार है, उसके बाद उस रचना के पीछे रचनाकार का क्या उद्देश्य है? उसे जाना जाए।
2. भाषा
जैसे विचार होते है, वैसे ही भाषा भी होती है। इसके अलावा भाषा विषय-वस्तु के चुनाव पर भी निर्भर करती है। विषय और वस्तु जिन परिस्थितियों पर आधारित होते है, भाषा भी उसी के अनुरूप होती है।
प्रत्येक रचनाकार की अपनी भाषा होती है। भाषा-संबंधी अध्ययन के लिए पर्यायवाची शब्द का अध्ययन, लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे और तत्सम शब्दों तथा तद्भव शब्दों का अध्ययन आवश्यक है।
3. शैली
गद्य रचना में शैली का काफी महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक ही विषय पर अलग-अलग रचनाकारों द्वारा लिखी गई बातें शैली अलग होने के कारण अलग-अलग हो जाती है। इसलिए, गद्य साहित्य में शैली का अध्ययन काफी आवश्यक होता है। हिंदी गद्य में कुछ प्रचलित शैलियों को नीचे बताया गया है।
(i). वर्णनात्मक शैली
वर्णनात्मक शैली का लक्ष्य किसी वस्तु अथवा व्यापार का वर्णन करना होता है। इसके द्वारा विषय की सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है।
(ii). विचारात्मक शैली
विचारात्मक शैली के द्वारा रचनाकार अपने विचारों को पाठकों के मन में बैठाने का प्रयास करता है। इस शैली के लिए बातें स्पष्ट होनी आवश्यक होती है। इसलिए, इसकी भाषा साफ, सरल और स्पष्ट होती है।
(iii). कथात्मक शैली
कथात्मक शैली का लक्ष्य अपने विचारों को कहानी के माध्यम से बताना होता है। इसलिए, कथात्मक शैली की भाषा आसान होती है।
(iv). भावात्मक शैली
भावात्मक शैली के द्वारा खुशी, करुणा, क्रोध, दुख, आदि भावना की कामना करने का प्रयास किया जाता है। गद्य का अध्ययन करते समय कभी-कभी अलंकारों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कविता की भांति गद्य में भी रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, आदि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है।
गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएँ
हिंदी गद्य को 4 विशाल भागों में विभक्त किया है, जो कि निम्न प्रकार है:-
| गद्य साहित्व की प्रमुख विधाएँ |
|---|
| कथा साहित्य |
| नाटक |
| निबंध |
| नवीन अथवा नई विधाएँ |
1. कथा साहित्य
कथा साहित्य में हम उपन्यास कहानी तथा लघु कथा पढ़ते है। यदि आपको अपने पढ़ने की गति तेज करनी है, तो गद्य में अधिक से अधिक कहानी और उपन्यास पढ़ने की कोशिश करें।
(i). कहानी
जीवन और समाज की किसी भी घटना का सुंदर ढंग से चित्रण करना ही ‘कहानी’ कहलाता है। कहानी में कथा का होना आवश्यक होता है। इसमें विचार सीधे-सीधे प्रकट न होकर किसी घटना के माध्यम से प्रकट होते है।
मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेंद्र, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, आदि हिंदी के कईं प्रमुख कहानीकार है।
(ii). उपन्यास
उपन्यास में भी जीवन और समाज में घटती हुई घटनाओं का वर्णन होता है, लेकिन उपन्यास में कहानी की तुलना में अधिक विस्तारपूर्वक से कथा का वर्णन किया जाता है। कहानी किसी एक घटना पर आधारित होती है, जबकि उपन्यास में कईं घटनाएँ होती है।
मुंशी प्रेमचंद, इलाचंद्र जोशी आचार्य, चतुरसेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, फणीश्वर नाथ रेणु, भगवती चरण शर्मा, यशपाल, अज्ञेय, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, विवेकी राय कमलेश्वर, आदि हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार है।
2. नाटक
नाटक में भी कहानी प्रमुख होती है, लेकिन इसमें कहानी की भांति घटनाओं का वर्णन नहीं होता है, बल्कि उस कहानी के पात्रों द्वारा अभिनय के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया जाता है।
इसलिए, यह आसानी से मनुष्य को समझ में आ जाता है। नाटक में लेखक जो भी बात कहना चाहता है, वह पात्रों के माध्यम से कहलवाता है।
3. निबंध
निबंध को गद्य-लेखन की कसौटी माना जाता है। निबंध का अर्थ:- ‘बिना बंधन के’ होता है अर्थात किसी विषय पर लिखते समय विचारों पर कोई बंधन नहीं होता है, तो वह रचना ‘निबंध’ कहलाती है।
निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध और लेख में अंतर होता है, लेख सिर्फ अपने विषय पर ही केंद्रित होता है, जबकि निबंध में विषय सिर्फ एक माध्यम भर होता है।
सभी नवीन विधाएँ निम्न प्रकार है:-
(i). यात्रा वृतांत
यात्रा वृतांत में लेखक किसी देश, पहाड़ अथवा किसी अन्य स्थान की अपनी यात्रा का अनुभव लिखता है। यात्रा के दौरान वह जैसा अनुभव करता है, उन सभी का वर्णन ही ‘यात्रा वृतांत’ कहलाता है।
राहुल सांकृत्यायन का ‘घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ’ प्रसिद्ध यात्रा ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त यशपाल, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, मनोहर श्याम जोशी, हिमांशु जोशी, आदि ने भी कईं यात्रा वृतांत लिखे है।
(ii). संस्मरण
किसी व्यक्ति अथवा स्थान का स्मरण करना ही ‘संस्मरण’ कहलाता है। संस्मरण में किसी व्यक्ति से अधिक भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण उससे जुड़ी हुई यादों तथा घटनाओं का वर्णन होता है।
(iii). व्यंग्य
समाज में फैली हुई बुराई, विचार, परंपरा अथवा किसी घटना का वर्णन करते हुए यदि उसका मजाक उड़ाया जाए और मजाकिया भाषा में उसका चित्रण किया जाए, तो वह रचना ‘व्यंग्य’ कहलाती है।
व्यंग्य में कहानी भी हो सकती है और निबंध की भांति स्वतंत्र विचार भी हो सकते है। व्यंग्य एक प्रकार का निबंध होता है, जिसमें व्यंगात्मक ढंग से किसी विषय का चित्रण किया जाता है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गोपाल चतुर्वेदी, आदि प्रमुख व्यंगकार है।
(iv). संपादकीय
पत्र अथवा पत्रिका के संपादक द्वारा जो कुछ लिखा जाता है, उसे ‘संपादकीय’ कहते है। प्रत्येक पत्र-पत्रिकाओं में एक ‘संपादकीय’ अवश्य होता है। संपादकीय में संपादक वर्तमान समय में चल रही समस्याओं तथा घटनाओं पर अपने विचार प्रकट करता है।
गद्य साहित्य का अध्ययन कैसे करें?
गद्य साहित्य का अध्ययन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:-
- गद्य साहित्य पढ़ने से पहले पुस्तक की भूमिका और परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि गद्य में सारांश दिया गया है, तो उसे भी पढ़ लेना चाहिए। इससे विषय को पढ़ने और समझने में सहायता मिलती है।
- गद्य के प्रथम तथा अंतिम अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि गद्य के प्रथम तथा अंतिम अनुच्छेद में मुख्य बातें बताई जाती है।
- गद्य पढ़ते समय विराम चिन्ह का ध्यान रखते हुए रुक-रुककर पढ़ना चाहिए।
- गद्य पढ़ते समय बीच में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में रुकने से क्रम बिगड़ जाता है और विषय समझ में नहीं आता है। इसलिए, तेज गति से पढ़ने की आदत डालें।
गद्य काव्य तथा पद्य काव्य में अंतर
गद्य काव्य तथा पद्य काव्य में सभी अंतर निम्नलिखित है:-
| गद्य | पद्य |
|---|---|
| गद्य काव्य में लयात्मकता नहीं होती है। | पद्य काव्य में लयात्मकता होती है अर्थात हम इन्हें सुर के साथ गा सकते है। |
| गद्य का संबंध हमारे विचारों से होता है। | पद्य का संबंध हमारे मन की भावनाओं से होता है। |
| गद्य का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। | पद्य का संबंध हमारे मन से होता है। |
| गद्य विद्या के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, व्यंग्य, आत्मकथा, पत्र, आदि आते है। | पद्य के अंतर्गत कविता, गीत, गाना, आदि आते है। |
| गद्य में अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाता है। | पद्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। |
| गद्य को पढ़ना काफी आसान होता है। | पद्य को पढ़ना गद्य की तुलना में मुश्किल होता है। |
गद्य काव्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
-
गद्य काव्य की परिभाषा क्या है?
मनुष्य के बोलने, लिखने व पढ़ने की छंदरहित साधारण व्यवहार की भाषा को ‘गद्य काव्य’ कहते है।
रोजमर्रा के जीवन में हम बातचीत करने, पत्र लिखने, अपने विचार प्रकट करने, प्रार्थना पत्र आदि को भेजने के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते है, वह भाषा का गद्य रूप ही होता है।
गद्य की भाषा सरल और आसानी से समझने लायक होती है, जबकि काव्य की भाषा विशेष होती है। गद्य की भाषा आसान होने के कारण हम अपने विचार आसानी से व्यक्त कर पाते है।
यही कारण है कि काव्य की अपेक्षा गद्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। आज निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृतांत, समाचार पत्र, संपादकीय, आदि गद्य के माध्यम से ही पढ़े-लिखे जाते है। इस प्रकार गद्य मानव जीवन में बहुत महत्व रखता है। -
गद्य काव्य के कितने अव्यय है?
पद्य काव्य के कुल 3 अव्यय है, जो कि निम्नलिखित है:-
1. विचार तत्व
2. भाषा
3. शैली -
गद्य साहित्य की कितनी विधाएँ है?
गद्य साहित्य की कुल 4 विधाएँ है, जो कि निम्नलिखित है:-
1. कथा साहित्य
2. नाटक
3. निबंध
4. नवीन विधाएँ
अंतिम शब्द
अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।
अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ फेसबुक पर साझा अवश्य करें और हमारे वेबसाइट को सबस्क्राइब कर ले।